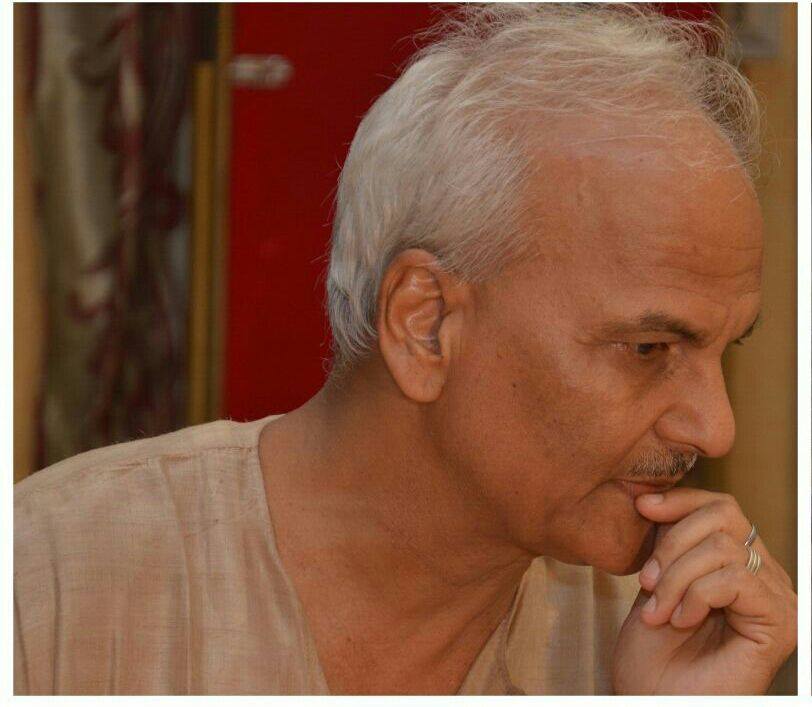बाहर कम
अधिक- अधिक भीतर
कायम है डर
घने अँधेरे में
दीख जाती है औचक
सामने कोई रस्सी
सिहर जाता है सर्वांग
‘बाप रे साँप !’
गेंहुअन की शक्ल में
सरकने लगती है रस्सी
हमारी ओर
डर हो जाता है अछोर
अँधेरी रात में
निर्जन राह का ठूँठ
बन जाता है पिशाच
ठोंकता है ताल
पाँवों को छूटने लगता है पसीना
बहुत बुरा हाल !
अँधेरा भ्रम का जनक
भय का संरक्षक है
हम बालते रहे हैं दीप
थामते रहे हैं मशाल
कहाँ थमा ,थका है अँधेरा
बढ़ता गया है तिमिर-जाल !!
भीतर ही भय डाले डेरा है
व्यंग्य कर रहा जैसे
‘दीपक तले ही अँधेरा है !’
कोयला खदानों में
कल-कारखानों में
जंगल , मैदानों में
निर्भय हम खटते हैं
कोड़ते हैं मिट्टी
तोड़ते हैं पत्थर
उनसे ही क्यों आख़िर
जाते हैं सहम ,डर ?
उनसे – जो डरते हैं
टर्राते काग से
रोती हुई बिल्ली से
बाँयें की छींक
और छत की छिपकली से
मालिक की धौंस
और हाकिम का हौव्वा
भागें तो कहाँ-कहाँ
भुगतें भी कबतक ?
भीतर के भय से ही
लड़ना है जैसे हो
चोटें अचूक
सिर्फ उसकी ही जड़ पर
बाहर के भय से
निजात तभी संभव है
आदमी को आदमी से
कैसा डर ? कैसा डर!